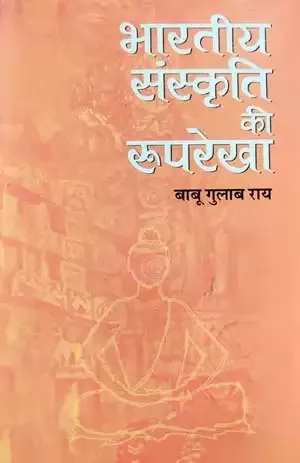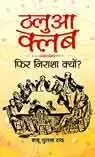|
संस्कृति >> भारतीय संस्कृति की रूपरेखा भारतीय संस्कृति की रूपरेखाबाबू गुलाबराय
|
277 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है पुस्तक भारतीय संस्कृति की रूपरेखा ...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कुछ सम्मतियाँ
साप्ताहिक हिंदुस्तान, नई दिल्ली
‘‘इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त रूप से
परिचय
देने का सराहनीय प्रयास है। भारतीय संस्कृति के विहंगम परिचय के लिए
पुस्तक बड़ी उपयोगी है।’’
15 मार्च 1953
अमृत पत्रिका, इलाहाबाद
‘‘प्रस्तुत पुस्तक में आपके गहन अध्ययन एवं घोर चिंतन
का
परिचय मिलता है पुस्तक सब प्रकार से सुन्दर बन पड़ी
है।’’
अप्रैल 1953
धर्मयुग, बंबई
‘‘कम समयवाले और पकी-पकाई सामग्री के इच्छुक पाठकों
के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है।’’
9 मार्च, 1953
सरस्वती, इलाहाबाद
‘‘भारतीय संस्कृति पर संक्षिप्त रूप से इस पुस्तक में
विद्वान् लेखक ने अच्छा प्रकाश डाला है, जो छात्रों के लिए विशेष रूप से
उपयोगी है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों और विभिन्न संस्कृतियों के
सम्मिश्रण का इसमें अच्छा विवेचन किया गया है ।’’
मई 1943
आत्म-निवेदन
यद्यपि संस्कृति का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसमें साहित्य, संगीत, कला,
धर्म, दर्शन, लोकवार्त्ता राजनीति- सभी का समावेश होता है, तथापि वह मूल
रूप से इतिहास का अंग है। इतिहास में अभी तक राजनीति को ही विशेष महत्त्व
दिया जाता रहा है और राजा-महाराजा, वीर सेनानी आदि ही इतिहास के वास्तविक
सूत्रधार माने जाते रहें हैं; किन्तु किसी देश की वास्तविक समृद्धि और
सम्पन्नता उसके नैतिक उन्नति, जीवन-यापन के स्तर, व्यवसायियों, संस्थाओं,
शिक्षा-दीक्षा और सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त कवियों,
विचारकों, कलाकारों, और जनता जनार्धन को भी स्थान मिलता है। राजनीति की
प्रवर्तक तो जनता की विचारधारा है। इसलिये अब इतिहास को भी महत्त्व दिया
जाने लगा है। यह परिवर्तन दृष्टिकोण पाठकों को देश के शरीर से ही नहीं
वरन् आत्मा से भी परिचित करा देगा और उनको जन-जीवन का भी निकटतम संम्पर्क
करा सकेगा।
‘भारत का सांस्कृतिक इतिहास’ लिखने के लिए उसके सागर के से विस्तार और गांभीर्य को एक छोटी सी पुस्तक के आकार में बाँधने के लिये जितना विविध विषयक ज्ञान अपेक्षित है उतना एक साधारण से मनुष्य में होना असंभव –सा है। इस संबंध में अपने सीमाओं का पूर्ण अनुभव रखते हुए भी मैंने भारतीय संस्कृति पर पुस्तक लिखने का जो साहस किया, वह कविकुल गुरू कालिदास के ‘तितीर्षर्दुस्तरं मोहदुडुपेनस्मि सागरम्’ से (अज्ञानवश घड़ों की नाव के सहारे दुस्तर सागर को पार करने का इच्छुक होना) कहीं अधिक था।
(दुःसाहस में तो कालिदास से भी बढ़ा-चढ़ा हो ही सकता हूँ) अस्तु मुझे इस महासागर को पार करने के लिये कुछ ऐसे लेखकों का आवलंबन लेना पड़ा कि जो इस कार्य में मुझसे कुछ अधिक सफल रहे हैं। उनमें से कुछ के नाम तथा उनकी कृतियों के नाम इस प्रकार हैं- श्री रामगोविंद त्रिवेदी कृत ‘वैदिक साहित्य’, श्री चंद्रशेखर शास्त्री लिखित ‘संस्कृत साहित्य की रूपरेखा’, श्री जयचंद्र विद्यालंकार रचित ‘संस्कृत वाङ्मय के अमर रत्न’, डॉ, बेनीप्रसाद प्रणीत ‘हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता’, श्री हरिदत्त विद्यालंकार रचित ‘भारत का सांस्कृतिक इतिहास’, ‘कल्याण का संस्कृति अंक’, ‘श्री रामकृष्ण परमहंस स्मारक ग्रन्थ’ ‘Cultural Heritage of India Vol. III’, श्री नरेन्द्र नाथ लॉ महोदय की ‘Hindu Polity ’, डॉ यदुनाथ सरकार की ‘India through ages’, श्रीमती अक्षय कुमारी देवी लिखित ‘The fundamentals of Hindu Sociology’, श्री अंबिकादत्त बाजपेई लिखित ‘हिन्दू राजस्व’ डॉ गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा लिखित, ‘मध्यकालीन भारतीय संस्कृति’ डॉ. श्यामसुंदर दास प्रणीत ‘हिंदी भाषा और साहित्य’ प्रमुख हैं, इनके अतिरिक्त ‘क्वचिदन्यतोऽपि के साथ रामायण, महाभारत, काव्य, स्मृतियों आदि के चंचुप्रहारी निजी अध्ययन ने कुछ हाथ-पैर पीटने में सहारा दिया है। ऊपर जिन महानुभावों की नामावली दी है, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। पाठकगण विशेषकर विद्यार्थी पाठक, विषय के पूर्ण ज्ञान के लिये इन पुस्तकों का यथासमय अध्ययन कर अपने कर्तव्य को पूर्णतया पालन करेंगे।
इतिहास में मौलिकता के लिए विशेष स्थान नहीं रहता। इतिहासकार की कल्पना और मौलिकता सत्य की लौह-श्रृंखला से बँधी रहती है, फिर भी उसमें बहुत कुछ अनुमान और तर्क से काम लिया जाता है। इतिहास में भी कुछ वैज्ञानिक रूढ़ियों के विरुद्ध जो मत अब प्रचार में आ रहे हैं, इस पुस्तक में उनकों भी समुचित आदर दिया जाता है। किन्तु प्रचलित और सामान्य मतों से विद्यार्थियों और सम्मान्य पाठकों को अनभिज्ञ नहीं रखा गया है। जहाँ तक हो सका है, एक विस्तृत क्षेत्र को इस पुस्तक के घेरे में बाँधने का प्रयत्न किया गया है, किंतु पुस्तक के सीमित आकार और अपनी अल्पज्ञता के कारण बहुत से विषयों को छोड़ना पडा, उसका मुझे वास्तविक खेद है। उदाहरणतया, दक्षिण की कला के साथ दक्षिण के साहित्य का भी परिचय देना चाहिए था; लोकवार्त्ता, रीति-रिवाज, मेले-तमाशे, रहन-सहन का थो़ड़ा –बहुत ज्ञान होते हुए इन विषयों के समावेश करने का मोह स्थानाभाव के कारण छोड़ना पड़ा। इसमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि एक साधारणतया विदग्ध पुरुष को अपने देश की संस्कृति के बारे में जितना ज्ञान नितांत आवश्यक है उतना दिया जा सके।
संस्कृति साहित्य के संबंध में हमारे विद्यार्थियों को बहुत कम ज्ञान रहता है। उसका दिग्दर्शन कराने के साथ-साथ उसमें पाए जानेवाले सांस्कृतिक तत्त्वों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत साहित्य पर आधारित तथ्यों की पुष्टि के लिये उपयुक्त उदारण भी दिये गए हैं। इसमें इतिहास के विद्यार्थियों को साहित्य से जितना सीधा संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, संपर्क को उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार कला के संबंध में भी दिशा-निर्देश मात्र किया गया है। कुछ कलाकृतियों के चित्र भी दिए गए हैं। पुस्तकों में जो तथ्य सामने रखे गए हैं, वे साहित्यकता के साथ उनकों शुष्क वैज्ञानिकता से बचाते हुए रखे गये हैं। मैं इस आशा से कि साधारण पाठक और विद्यार्थी इस पुस्तक को अपने मानसिक क्षितिज के विस्तार के लिये अपनाएँगे, इसको उनके हाथों में सप्रेम सौंपता हूँ। मैं शिक्षित समुदाय का विशेष अनुगृहीत हूँ कि इसका पुस्तक का द्वितीय संस्करण उनको समर्पण करने का अवसर मिल रहा है।
‘भारत का सांस्कृतिक इतिहास’ लिखने के लिए उसके सागर के से विस्तार और गांभीर्य को एक छोटी सी पुस्तक के आकार में बाँधने के लिये जितना विविध विषयक ज्ञान अपेक्षित है उतना एक साधारण से मनुष्य में होना असंभव –सा है। इस संबंध में अपने सीमाओं का पूर्ण अनुभव रखते हुए भी मैंने भारतीय संस्कृति पर पुस्तक लिखने का जो साहस किया, वह कविकुल गुरू कालिदास के ‘तितीर्षर्दुस्तरं मोहदुडुपेनस्मि सागरम्’ से (अज्ञानवश घड़ों की नाव के सहारे दुस्तर सागर को पार करने का इच्छुक होना) कहीं अधिक था।
(दुःसाहस में तो कालिदास से भी बढ़ा-चढ़ा हो ही सकता हूँ) अस्तु मुझे इस महासागर को पार करने के लिये कुछ ऐसे लेखकों का आवलंबन लेना पड़ा कि जो इस कार्य में मुझसे कुछ अधिक सफल रहे हैं। उनमें से कुछ के नाम तथा उनकी कृतियों के नाम इस प्रकार हैं- श्री रामगोविंद त्रिवेदी कृत ‘वैदिक साहित्य’, श्री चंद्रशेखर शास्त्री लिखित ‘संस्कृत साहित्य की रूपरेखा’, श्री जयचंद्र विद्यालंकार रचित ‘संस्कृत वाङ्मय के अमर रत्न’, डॉ, बेनीप्रसाद प्रणीत ‘हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता’, श्री हरिदत्त विद्यालंकार रचित ‘भारत का सांस्कृतिक इतिहास’, ‘कल्याण का संस्कृति अंक’, ‘श्री रामकृष्ण परमहंस स्मारक ग्रन्थ’ ‘Cultural Heritage of India Vol. III’, श्री नरेन्द्र नाथ लॉ महोदय की ‘Hindu Polity ’, डॉ यदुनाथ सरकार की ‘India through ages’, श्रीमती अक्षय कुमारी देवी लिखित ‘The fundamentals of Hindu Sociology’, श्री अंबिकादत्त बाजपेई लिखित ‘हिन्दू राजस्व’ डॉ गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा लिखित, ‘मध्यकालीन भारतीय संस्कृति’ डॉ. श्यामसुंदर दास प्रणीत ‘हिंदी भाषा और साहित्य’ प्रमुख हैं, इनके अतिरिक्त ‘क्वचिदन्यतोऽपि के साथ रामायण, महाभारत, काव्य, स्मृतियों आदि के चंचुप्रहारी निजी अध्ययन ने कुछ हाथ-पैर पीटने में सहारा दिया है। ऊपर जिन महानुभावों की नामावली दी है, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। पाठकगण विशेषकर विद्यार्थी पाठक, विषय के पूर्ण ज्ञान के लिये इन पुस्तकों का यथासमय अध्ययन कर अपने कर्तव्य को पूर्णतया पालन करेंगे।
इतिहास में मौलिकता के लिए विशेष स्थान नहीं रहता। इतिहासकार की कल्पना और मौलिकता सत्य की लौह-श्रृंखला से बँधी रहती है, फिर भी उसमें बहुत कुछ अनुमान और तर्क से काम लिया जाता है। इतिहास में भी कुछ वैज्ञानिक रूढ़ियों के विरुद्ध जो मत अब प्रचार में आ रहे हैं, इस पुस्तक में उनकों भी समुचित आदर दिया जाता है। किन्तु प्रचलित और सामान्य मतों से विद्यार्थियों और सम्मान्य पाठकों को अनभिज्ञ नहीं रखा गया है। जहाँ तक हो सका है, एक विस्तृत क्षेत्र को इस पुस्तक के घेरे में बाँधने का प्रयत्न किया गया है, किंतु पुस्तक के सीमित आकार और अपनी अल्पज्ञता के कारण बहुत से विषयों को छोड़ना पडा, उसका मुझे वास्तविक खेद है। उदाहरणतया, दक्षिण की कला के साथ दक्षिण के साहित्य का भी परिचय देना चाहिए था; लोकवार्त्ता, रीति-रिवाज, मेले-तमाशे, रहन-सहन का थो़ड़ा –बहुत ज्ञान होते हुए इन विषयों के समावेश करने का मोह स्थानाभाव के कारण छोड़ना पड़ा। इसमें इस बात का प्रयत्न किया गया है कि एक साधारणतया विदग्ध पुरुष को अपने देश की संस्कृति के बारे में जितना ज्ञान नितांत आवश्यक है उतना दिया जा सके।
संस्कृति साहित्य के संबंध में हमारे विद्यार्थियों को बहुत कम ज्ञान रहता है। उसका दिग्दर्शन कराने के साथ-साथ उसमें पाए जानेवाले सांस्कृतिक तत्त्वों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत साहित्य पर आधारित तथ्यों की पुष्टि के लिये उपयुक्त उदारण भी दिये गए हैं। इसमें इतिहास के विद्यार्थियों को साहित्य से जितना सीधा संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, संपर्क को उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार कला के संबंध में भी दिशा-निर्देश मात्र किया गया है। कुछ कलाकृतियों के चित्र भी दिए गए हैं। पुस्तकों में जो तथ्य सामने रखे गए हैं, वे साहित्यकता के साथ उनकों शुष्क वैज्ञानिकता से बचाते हुए रखे गये हैं। मैं इस आशा से कि साधारण पाठक और विद्यार्थी इस पुस्तक को अपने मानसिक क्षितिज के विस्तार के लिये अपनाएँगे, इसको उनके हाथों में सप्रेम सौंपता हूँ। मैं शिक्षित समुदाय का विशेष अनुगृहीत हूँ कि इसका पुस्तक का द्वितीय संस्करण उनको समर्पण करने का अवसर मिल रहा है।
विनीत गुलाबराय
भारतीय संस्कृति की रूपरेखा
शब्द का अर्थ- ‘संस्कृति’ शब्द
का संबंध संस्कार
जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना।
‘संस्कृति’ शब्द का भी यही अर्थ है। अंग्रेजी शब्द
कल्चर में
वही धातु है जो ‘एग्रीकल्चर में हैं। इसका भी अर्थ पैदा करना या
सुधारना’ है। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी।
जातीय
संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। भाववाचन होने के कारण
‘संस्कृति’ एक समूहवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल
रहन-सहन को
विधियों और विचार-परंपराओं के, जाति के लोगों में दृढ़मूल हो
जाने
से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति
के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता
है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित
होते हैं। मनुष्य अकेला रहने पर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। ये संस्कार
दूसरे देश में निवास करने तथा दूसरे देशवासियों के सम्पर्क में आने से कुछ
परिवर्तित भी हो सकते हैं और कभी-कभी दब भी जाते हैं। किंतु अनुकूल
वातावरण प्राप्त करने पर फिर उभर आते हैं।
धर्म और संस्कृति – धर्म में भी प्रायः वे ही संस्कार आते है जो संस्कृति में हैं। हमारे यहाँ ‘धर्म’ व्यापक शब्द है। वह सारे जीवन को शासित करता है। धर्म और संस्कृति में अंतर केवल इतना ही है कि धर्म में श्रुति, स्मृतियों और पुराण ग्रंथों का आधार रहता है। किंतु संस्कृति में परंपरा का आधार रहता है। धर्म और संस्कृति का कोई विरोध नहीं है। धर्म देश-निरपेक्ष है, किंतु संस्कृति का संबंध देश से अधिक है। मुसलमानों में पृथक रहने की प्रवृत्ति अवश्य है, फिर भी उन्होंने देश की संस्कृति और रीति-रिवाजों को बहुत कुछ अपनाया है।
धर्म और संस्कृति – धर्म में भी प्रायः वे ही संस्कार आते है जो संस्कृति में हैं। हमारे यहाँ ‘धर्म’ व्यापक शब्द है। वह सारे जीवन को शासित करता है। धर्म और संस्कृति में अंतर केवल इतना ही है कि धर्म में श्रुति, स्मृतियों और पुराण ग्रंथों का आधार रहता है। किंतु संस्कृति में परंपरा का आधार रहता है। धर्म और संस्कृति का कोई विरोध नहीं है। धर्म देश-निरपेक्ष है, किंतु संस्कृति का संबंध देश से अधिक है। मुसलमानों में पृथक रहने की प्रवृत्ति अवश्य है, फिर भी उन्होंने देश की संस्कृति और रीति-रिवाजों को बहुत कुछ अपनाया है।
दो पक्ष-
संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आतंरिक भी। उसका बाह्य पक्ष आंतरिक
का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। हमारे बाह्य आचार हमारे
विचारों और मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं। यद्यपि संस्कृति का मूल
आधार मानवता है तथापि देश विशेष के वातावरण की विशेषता के कारण वह इस देश
के नाम से जैसे-भारतीय संस्कृति, ईरानी संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति आदि
नामों से विदित होने लगती है। संस्कृति का एक ही मूल उद्देश्य मानते है
हुए भी हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति देश विदेश की उपज होती है, उसका
संबंध देश के भौतिक वातावरण और उसमें पालित, पोषित एवं परिवर्द्धित
विचारों से होता है।
संस्कृति और सभ्यता – संस्कृति के बाह्य पक्ष को ही सभ्यता कहते है। सभ्यता मूल में तो व्यवहार की साधुता के द्योतक होती है। (सभायां साधवः- सभ्या) किंतु अर्थ-विस्तार से यह शब्द रहन-सहन की उच्चता तथा सुखयम जीवन व्यतीत करने के साधनों, जैसे-कला-कौशल, स्थापत्य, ज्ञान-विज्ञान की उन्नति पर लागू होता है। किंतु आजकल इस शब्द के प्रयोग में बहुत स्थूलता आ गई है। आजकल तो सभ्यता का मापदंड साबुन या सल्फ्यूरिक एसिड की खपत हो गया है किंतु बात सोलह आने ऐसी नहीं है जिस सभ्यता का आधार संस्कृति में नहीं, वह सभ्यता नहीं। संस्कृति की आत्मा के बिना सभ्यता का शरीर शिव की भाँति निष्प्राण रहता है। विनय और शील के बिना कटी-छँटी पोशाक, सुसज्जित बँगले सेंट और पाउडर मनुष्य को सभ्य नहीं बना सकते। विनय और शील के बाहरी रूप को ही भ्रष्टाचार्य कहते हैं, किन्तु यह भी दिखावा मात्र नहीं है। शिष्टाचार का अर्थ है शिष्टों का आचरण, किंतु इसमें रूढ़ि या परंपरा की भावना लगी रहती है।
संस्कृति और सभ्यता – संस्कृति के बाह्य पक्ष को ही सभ्यता कहते है। सभ्यता मूल में तो व्यवहार की साधुता के द्योतक होती है। (सभायां साधवः- सभ्या) किंतु अर्थ-विस्तार से यह शब्द रहन-सहन की उच्चता तथा सुखयम जीवन व्यतीत करने के साधनों, जैसे-कला-कौशल, स्थापत्य, ज्ञान-विज्ञान की उन्नति पर लागू होता है। किंतु आजकल इस शब्द के प्रयोग में बहुत स्थूलता आ गई है। आजकल तो सभ्यता का मापदंड साबुन या सल्फ्यूरिक एसिड की खपत हो गया है किंतु बात सोलह आने ऐसी नहीं है जिस सभ्यता का आधार संस्कृति में नहीं, वह सभ्यता नहीं। संस्कृति की आत्मा के बिना सभ्यता का शरीर शिव की भाँति निष्प्राण रहता है। विनय और शील के बिना कटी-छँटी पोशाक, सुसज्जित बँगले सेंट और पाउडर मनुष्य को सभ्य नहीं बना सकते। विनय और शील के बाहरी रूप को ही भ्रष्टाचार्य कहते हैं, किन्तु यह भी दिखावा मात्र नहीं है। शिष्टाचार का अर्थ है शिष्टों का आचरण, किंतु इसमें रूढ़ि या परंपरा की भावना लगी रहती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book